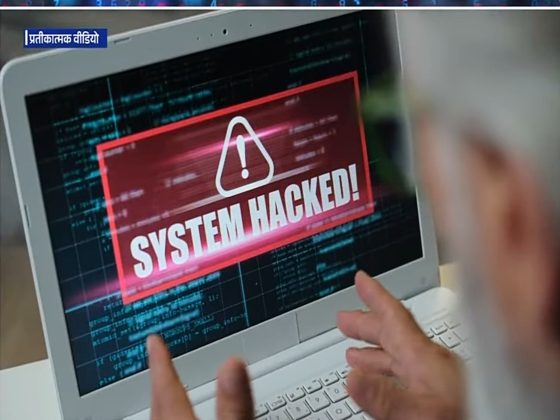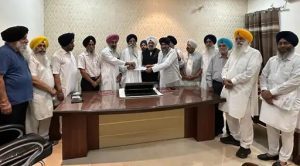अपराध का स्वरूप में तेज़ी से बदलाव-नेशनल अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) रिपोर्ट 30 सितंबर 2025 को जारी
भारत में मोबाइल चोरों ज़ेबक़टों साइबर क्राइम के अपराधियों को पब्लिक डोमेन में घुमाना समय की मांग-जनता इन्हें पहचान कर सतर्क रहे-एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र
गोंदिया-भारत में अपराध का स्वरूप पिछले कुछ वर्षों में तेज़ी से बदल रहा है। पारंपरिक हिंसक, अपराधों में जहाँ कुछ गिरावट देखी जा रही है,वहीं तकनीक आधारित अपराध, विशेषकर साइबर अपराध, उभरकर सामने आ रहे हैं और आम नागरिकों के लिए नए-नए खतरे पैदा कर रहे हैं।30 सितंबर 2025 को जारी अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) रिपोर्ट 2023 के आँकड़ों ने इस बदलाव की भयावहता को स्पष्ट कर दिया है-पूरे देश में साइबर अपराधों की संख्या में एक वर्ष में लगभग 31फ़ीसदीं की लगाकर 86,420 मामले दर्ज किए गए हैं,यह केवल आँकड़ा नहीं,बल्कि डिजिटल युग में भरोसे की टूटन और संस्थागत तैयारियों की कमज़ोरी का प्रतीक भी है। यह भी देखा गया है कि राष्ट्रीय औसत के पीछे राज्यों की असमान भागीदारी है-कुछ राज्य (विशेषकर कर्नाटक और तेलंगाना) में केसों की भारी तादाद है।कर्नाटक में21,889 और तेलंगाना में 18,236 साइबर अपराध दर्ज किए गए; पाँच राज्यों,कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार,ने मिलकर लगभग तीन- चौथाई साइबर मामलों का बोझ उठाया। जनसंख्या के अनुपात में तेलंगाना शीर्ष पर है, जहाँ प्रति लाख आबादी पर 47.8 मामले दर्ज हुए, जबकि राष्ट्रीय दर 6.2 प्रति लाख तक पहुँच गई (2022 में 4.8 थी)। इन आँकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि समस्या न केवल संख्यात्मक है, बल्कि भौगोलिक रूप से भी केंद्रीकृत है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र मानता हूं कि शहरी और सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले पारंपरिक चोरियों के तरीके आज अधिक परिष्कृत और नेटवर्केड बन गए हैं। मोबाइल-चोरी जेबक़ाट और भीड़ में हाथ साफ कर देने जैसे अपराध अब केवल एक व्यक्ति की चालाकी नहीं रहे; ये अक्सर रैकेट, तकनीक और सोशल इंजीनियरिंग की मिली-जुली रणनीतियों पर आधारित होते हैं। मैंने स्वयं अनुभव किया कि जैसे हैदराबाद/सिकंदराबाद लोकल बसों में जेबकाट की घटनाएँ मेरे सामने हुई, इसी बदलते परिदृश्य का स्थानीय अनुभव हैं जहाँ अपराधी भीड़, ट्रैफ़िक और यात्रियों की निरक्षरता का लाभ उठाकर कम समय में बड़ी वारदात कर लेते हैं।तकनीक का दुरुपयोग बड़े पैमाने पर आर्थिक नुक़सान के लिए हो रहा है, और इसका सीधा असर उन नागरिकों पर पड़ रहा है जो डिजिटल सर्विसेज, नेट-बैंकिंग और मोबाइल वॉलेट का उपयोग करते हैं।
साथियों बात अगर हम क्यों बढ़ रहे हैं मोबाइल-चोरी और साइबर अपराध? इसको समझने की करें तो (क) डिजिटल पैंठ इंटरनेट- बैंकिंग,यूपी-आई,मोबाइल-वॉलेट ई-कॉमर्स और रिमोट-वर्क में तेजी से वृद्धि ने अधिक लेन-देन और डिजिटल पहचान के टुकड़ों की उपलब्धता बढ़ा दी,जो क्रिमिनल्स के लिए फायदा है।(ख)सोशल इंजीनियरिंग और धोखाधड़ी- लोगों की भरोसेमंदी और डिजिटल साक्षरता में कमी का फायदा उठाकर फ़िशिंग, वॉइस-फिशिंग और नकली वेबसाइट/ऑप-ऐप के जरिए पैसे निकाल लिए जाते हैं। (ग) भीड़ और सार्वजनिक परिवहन का अवसर-लोकल बसों, ट्रेन प्लेटफार्मों, भीड़-भाड़ वाले बाजारों में अपराधी हाथ की सफाई बड़ी तेज़ी से करते हैं,पीड़ित को महसूस होने पर तक़रीबन बहुत देर हो चुकी होती है।मेंरा हैदराबाद-लोकल अनुभव की तर्ज़ पर ऐसे कई स्थानों पर अपराधी एकदम चुपके से मोबाइल या नकद निकाल लेते हैं। (घ) लॉ इम्प्लीमेंटेशन – गैप-पुलिस और नियामक संस्थाओं की डिजिटल- विशेषज्ञता फास्ट-ट्रेसिंगक्षमता और क्रॉस-जुरिस्डिक्शनल समन्वय सीमित हैं, जिससे अपराधी अक्सर राज्यों के परे जाकर अलग-अलग तरीके अपनाकर बच निकलते हैं।(ङ) आर्थिक-सामाजिक कारण- बेरोज़गारी, असमानता और अपराध नेटवर्क की पेशेवर संरचना भी इस बढ़ती प्रवृत्ति के पीछे है,अपराधी छोटे-छोटे व्यक्तिगत अपराध से संगठनात्मक नेटवर्क तक विकसित हो रहे हैं।
साथियों बात अगर हम क्या अपराधियों को ‘पब्लिक डोमेन’ में घुमाना चाहिए? नैतिक, कानूनी और व्यावहारिक विचार को समझने की करें तो,मोबाइल चोरों, जेबकाटों और साइबर अपराधियों को सार्वजनिक रूप से घुमाया जाए ताकि जनता उन्हें पहचान सके और सतर्क रहे। यह सुझाव भावनात्मक रूप से समझने योग्य है, पीड़ितों की पीड़ा और नाखुशी इस तरह के कड़े कदमों के पीछे प्रेरक हो सकती है। पर इस विचार को लागू करने से पहले कई कानूनी, मानवाधिकार और सुरक्षा- आधारित प्रश्नों का समाधान ज़रूरी है।(1) किसी भी व्यक्ति की पहचान सार्वजनिक करने से पहले यह सैद्धान्तिक और कानूनी सिद्ध होना चाहिए कि वह अपराधी है,गिरफ्तारी, चार्जशीटिंग और अदालत द्वारा दोषसिद्धि से पहले सार्वजनिक पहचान करने से न्यायिक प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है और गलत गिरफ्तारियों से निर्दोष लोगों का जीवन तबाह हो सकता है। (2), सार्वजनिक लिंचिंग और सोशल-शेमिंग के खतरे हैं- प्रबंधन के बिना ऐसी नीतियाँ भीड़ द्वारा हिंसा को बढ़ावा दे सकती हैं।(3) निजता और मानवीय गरिमा के अधिकार अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के तहत संरक्षित हैं; राज्य को कानून के दायरे में ही कार्य करना चाहिए।फिर भी, ‘सार्वजनिक जानकारी’ और ‘जन-सुरक्षा सूचना’ के बीच संतुलन बनाना संभव है और ज़रूरी भी।कई लोकतांत्रिक देश और पुलिस-विभाग पीड़ित- सहायता और सार्वजनिक चेतावनी के लक्ष्य से सीमित, नियंत्रित और न्यायिक अनुमति पर अपराधियों/संदिग्धों की तस्वीरें जारी करते हैं,जैसे कि गिरफ्तारी के बाद ‘वांटेड’ सूचनाएँ, सीसीटीवी फुटेज, और सक्रिय चेतावनी संदेश। इस तरह के कदम पारदर्शिता, सावधानी और कानूनी मंज़ूरी से किए जाएँ तो वे उपयोगी साबित हो सकते हैं,पर उनके साथ कानून को शर्तें भी लागू हो सकती है।
साथियों बात अगर हम व्यावहारिक विकल्प जो केंद्र और राज्य गृह विभाग के स्तरपर तुरंत लागू किए जा सकते हैं इसको समझने की करें तो (1) स्मार्ट-वांटेड पोर्टल और मोबाइल अलर्ट्स- पुलिस को एक केंद्रीकृत पोर्टल और मोबाइल अलर्ट सिस्टम चाहिए, जहाँ गिरफ्तारी/जांच के बाद, और न्यायिक मंज़ूरी के अनुरूप, स्थानीय रूप से अपराधियों की तस्वीरें और विवरण अपलोड किए जाएँ,ताकि जनता सचेत रहे। यह सिस्टम जीपीएस -आधारित अलर्ट भेजेगा जब कोई ‘उच्च-जोखिम क्रिमिनल’ किसी नगर के सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में दिखाई दे। (2) लोकल-गीत/ऑडियो-विजुअल जागरूकता अभियान: विशेषकर कम-शिक्षित और बुज़ुर्ग लोगों के लिए रेडियो, लोकल- बसों में पोस्टर और ऑडियो संदेश, जो जेबकाट से बचने, मोबाइल सुरक्षित रखने और नकद न दिखाने के व्यवहारिक उपाय बताते हों।(3) पुलिस-टेक स्किलिंग और साइबर- रैपिड- रिस्पॉन्स यूनिट- हर ज़िले में साइबर-विशेषज्ञों की टीम रखें जो धोखाधड़ी के डिजिटल निशानों को तुरंत ट्रेस कर सके और तत्काल कॉल/बैंक-फ्रीज़ जैसे कदम उठा सके।(4) रेल-और-बस सीसीटीवी- इंटीग्रेशन और पोर्टेबल-रैडार: भीड़-भाड़ वाले मार्गों पर उच्च-रिज़ॉल्यूशन सीसीटीवी व एएनपीआर सिस्टम, और संदिग्ध पैटर्न का एआई -आधारित अलर्ट, जिससे जेबकाट गैंग्स पहले पकड़े जा सकें।(5) तेज़-प्रति-राज्य समन्वय,-गैंग -आधारित अपराध अक्सर राज्यों के पार होते हैं; इसलिए मेटा-डेटा एक्सचेंज, त्वरित गिरफ्तारियों के लिए समन्वय और साझा फोरेंसिक प्लेटफॉर्म अत्यंत आवश्यक हैँ।
साथियों बात अगर हम मेरा अनुभव,हैदराबाद- सिकंदराबाद बसों में मोबाइल चोरी,जेबकटों की घटनाएं हुई इसको समझने की करें तो,मेरा अनुभव दर्शाता है कि लोकल बसों में जेबकाट- घटनाएँ सक्रिय हैं। इस स्थानीय स्तरपर तत्काल उपायों मेंशामिल होना चाहिए कि बसों में यात्रियों के लिए सुरक्षा-माइक/सीनल (ड्राइवर/ कंडक्टर हटाने का बटन), सीसीटीवी का इंस्टॉल और नियमित मॉनिटरिंग, यात्री- जागरूकता पोस्टर, और बस स्टैंड पर पुलिस-नाके, साथ ही, बसों के दौरान यात्रियों को सलाह दी जानी चाहिए कि, मोबाइल को अग्रभाग के अंदर जेब में रखें, बैक-पॉकेट और खुले हाथ में नकद न रखें, और भीड़ में बैग को शरीर के सामने रखें। स्थानीय ट्रैवल-अथॉरिटीज को यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता बनाना चाहिए और पुलिस- कम्प्लाइंट- काउंटरों को हर मुख्य स्टॉप पर सक्रिय रखना चाहिए।
साथियों बात अगर हम पीड़ित केंद्रित सेवाओं को समझने की करें तो,अक्सर पीड़ितों में शर्म, अनभिज्ञता या प्रक्रियागत जटिलताओं के कारण करीब 50फ़ीसदी से अधिक शिकायत दर्ज नहीं कराते। इसीलिए पीड़ित- केन्द्रित सेवाएँ ज़रूरी हैं-एक-स्टॉप-पॉइंट जहाँ पीड़ित एफआईआर, बैंक-रिपोर्ट, फॉरेंसिक-हेल्प,और साइबर- लॉजिस्टिक्स (जैसे स्टेटमेंट रिट्रीवल, बैंक टेलीकॉम ट्रैस) एक-साथ मिलें। इसके अलावा पीड़ित-काउंसलिंग और फास्ट-रिपेयर (बैंकों के साथ समझौते: फ्रॉड में फंड रीकवरी-स्टैंडर्ड) भी लागू किए जाने चाहिए।
साथियों बात अगर हम नीति- निर्माण के लिए केंद्र एवं राज्य के लिए प्रस्तावित रोडमैप को समझने की करें तो (1)कानूनी स्पष्टताऔरमानक-ऑपरेशनल-प्रोसीजर-जब पुलिस किसी अपराधी की पहचान सार्वजनिक करे, तो किन शर्तों पर और किस समय पर जानकारी जारी होगी इसका संसद/स्टेट लॉ-विभाग द्वारा नियमावलियाँ तय हों।(2)साइबर-फास्ट-ट्रेसिंग नेटवर्क: बैंक, टेक कंपनियों और पुलिस के बीच रीयल-टाइम डेटा-शेयरिंग एमओयू और एपी आई.(3) जन-जागरूकता मिशन: विद्यालय, वृद्धाश्रम, रेलवे, बस स्टेशनों पर सुसंगठित अभियान(4)साइबर-रैपिड-रिस्पॉन्स-फण्ड: पीड़ितों के लिए तात्कालिक वित्तीय सहायता और बैंकों के साथ सहमति द्वारा फंड का आंशिक क्लेम।(5)इंटर-स्टेट गैंग-बस्टिंग यूनिट: जेबकाट/रैकेट-ऑपरेशन के विरुद्ध संयुक्त कार्यनीति।(6)राज्य के साथ-साथ नागरिकों की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है। पड़ोस-निगरानी, सार्वजनिक- शिक्षा सेशन,और ‘सुरक्षित-यात्री’ स्वैच्छिक कार्यक्रम लोकल स्तर पर बहुत प्रभाव डाल सकते हैं। लोगों को सिखाना चाहिए कि वे किस तरह संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट करें, किस तरह बैंक/टेलीकॉम को तुरंत अलर्ट करें, और कैसे व्यक्तिगत डिजिटल- हैबिट्स बदलकर जोखिम कम कर सकते हैं।
अतः अगर हम उपरोक्त विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि मोबाइल चोरों, जेबकाटों और साइबर अपराधियों की बढ़ती दुस्साहसियत केवल पुलिस या सरकार का अकेला विषय नहीं है; यह समाज, टेक्नोलॉजी- कंपनियाँ, बैंकिंग-इंडस्ट्री और नागरिकों का संयुक्त संकट है। एनसीआरबी के हालिया आँकड़े 86,420 साइबर मामलों में 31फ़ीसदी की वृद्धि; राज्यवार असमानता; धोखाधड़ी का बढ़ता हिस्सा बतलाते हैं कि समस्या तेज़ी से गंभीर होती जा रही है और उसे बहु-आयामी नीतियों से ही रोका जा सकता है। ‘पब्लिक- डोमेन में घुमाना’ जैसा उपाय भावनात्मक समझदार हो सकता है पर उसे बिना सूचित कानूनी ढाँचे और सुरक्षा-गारंटी के लागू नहीं करना चाहिए,गलतियाँ और दमन दोनों का जोखिम वहाँ अधिक है।
*-संकलनकर्ता लेखक – क़र विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यमा सीए(एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र *